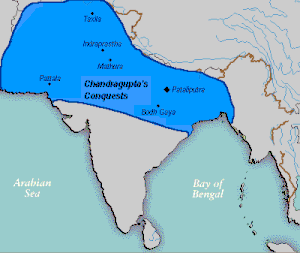चन्द्रगुप्त मौर्य
| जाती (कोइरी,शाक्य)चन्द्रगुप्त मौर्य | |
|---|---|
| सम्राट | |
 | |
| बिंदुसार | |
| राज्यकाल | ३२२ ईसा पूर्व-२९८ ईसा पूर्व |
| राज्याभिषेक | ३२२ ईसा पूर्व |
| पूर्वाधिकारी | नंद साम्राज्य के धनानंद |
| उत्तराधिकारी | बिन्दुसार |
| पत्नी | दुर्धरा और हेलेना (सेलुकस निकटर की पुत्री) |
| मातृ भाषा | संस्कृत/ प्राकृत |
| जन्म | 345 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र (अब बिहार में) |
| मृत्यु | 297 ईसा पूर्व (उम्र 41–42) श्रवणबेलगोला, कर्नाटक |
| सन्तान | बिन्दुसार |
| कुल | सूर्यवंशी |
चन्द्रगुप्त मौर्य (जन्म 345 ई॰पु॰, राज 322[1]-२९८ ई॰पु॰[2]) में भारत के सम्राट थे। इनको कभी कभी चन्द्रगुप्त नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चन्द्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफ़ल रहे। भारत राष्ट्र निर्माण मौर्य गणराज्य ( चन्द्रगुप्त मौर्य )
सम्राट् चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि साधारणतया ३२२ ई.पू. निर्धारित की जाती है। उन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत प्राय: २९८ ई.पू. में हुआ।
मेगस्थनीज ने चार साल तक चन्द्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएँ दी। ग्रीक और लैटिन लेखों में , चंद्रगुप्त को क्रमशः सैंड्रोकोट्स और एंडोकॉटस के नाम से जाना जाता है।
चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजा हैं। चन्द्रगुप्त के सिहासन संभालने से पहले, सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था, और 324 ईसा पूर्व में उसकी सेना में विद्रोह की वजह से आगे का प्रचार छोड़ दिया, जिससे भारत-ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्रों की विरासत सीधे तौर पर चन्द्रगुप्त ने संभाली। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य (जिसे कौटिल्य और विष्णु गुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जौ चन्द्र गुप्त के प्रधानमंत्री भी थे) के साथ, एक नया साम्राज्य बनाया, राज्यचक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा।[3]
चंद्रगुप्त मौर्य के वंशादि के बारे में अधिक ज्ञात नहीं है। जैन परिसिष्टपर्वन् के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य मयूरपोषकों के एक ग्राम के मुखिया की पुत्री से उत्पन्न थे। मध्यकालीन अभिलेखों के साक्ष्यानुसार मौर्य सूर्यवंशी मांधाता से उत्पन्न थे। बौद्ध साहित्य में मौर्य क्षत्रिय कहे गए हैं। महावंश चंद्रगुप्त कोमोरिय (मौर्य) खत्तियों से पैदा हुआ बताता है। दिव्यावदान में बिंदुसार स्वयं की मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय कहते हैं। सम्राट अशोक भी स्वयं को क्षत्रिय बताते हैं। महापरिनिब्बान सुत्त से 5 वी शताब्दी ई 0 पू 0 उत्तर भारत आठ छोटे छोटे गाणराज्यों में बटा था। मोरिय पिप्पलिवन के शासक, गणतांत्रिक व्यवस्थावाली जाति सिद्ध होते हैं। पिप्पलिवन ई.पू. छठी शताब्दी में नेपाल की तराई में स्थित रुम्मिनदेई से लेकर आधुनिक देवरिया जिले के कसया प्रदेश तक को कहते थे। मगध साम्राज्य की प्रसारनीति के कारण इनकी स्वतंत्र स्थिति शीघ्र ही समाप्त हो गई। यहीं कारण था कि चंद्रगुप्त का मयूरपोषकों, चरवाहों तथा लुब्धकों के संपर्क में पालन हुआ। परंपरा के अनुसार वह बचपन में अत्यंत तीक्ष्णबुद्धि था, एवं समवयस्क बालकों का सम्राट् बनकर उनपर शासन करता था। ऐसे ही किसी अवसर पर चाणक्य की दृष्टि उसपर पड़ी, फलत: चंद्रगुप्त तक्षशिला गए जहाँ उन्हें राजोचित शिक्षा दी गई। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के अनुसार सांद्रोकात्तस (चंद्रगुप्त) साधारणजन्मा था।
सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत धनानंद द्वारा शासित था। नंद सम्राट् अपनी निम्न उत्पत्ति एवं निरंकुशता के कारण जनता में अप्रिय थे। ब्राह्मण चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने राज्य में व्याप्त असंतोष का सहारा ले नंद वंश को उच्छिन्न करने का निश्चय किया अपनी उद्देश्यसिद्धि के निमित्त चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक विशाल विजयवाहिनी का प्रबंध किया ब्राह्मण ग्रंथों में नंदोन्मूलन का श्रेय चाणक्य को दिया गया है। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त डाकू था और छोटे-बड़े सफल हमलों के पश्चात् उसने साम्राज्यनिर्माण का निश्चय किया। अर्थशास्त्र में कहा है कि सैनिकों की भरती चोरों, म्लेच्छों, आटविकों तथा शस्त्रोपजीवी श्रेणियों से करनी चाहिए। मुद्राराक्षस से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा पर्वतक से संधि की। चंद्रगुप्त की सेना में शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसीक तथा वह्लीक भी रहे होंगे। प्लूटार्क के अनुसार सांद्रोकोत्तस ने संपूर्ण भारत को 6,00,000 सैनिकों की विशाल वाहिनी द्वारा जीतकर अपने अधीन कर लिया। जस्टिन के मत से भारत चंद्रगुप्त के अधिकार में था।
चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति पंजाब में सदृढ़ की। उसका यवनों विरुद्ध स्वातंत्रय युद्ध संभवत: सिकंदर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद आरंभ हो गया था। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के उपरांत भारत ने सांद्रोकोत्तस के नेतृत्व में दासता के बंधन को तोड़ फेंका तथा यवन राज्यपालों को मार डाला। चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियन लगभग 323 ई.पू. में आरंभ किया होगा, किंतु उन्हें इस अभियान में पूर्ण सफलता 317 ई.पू. या उसके बाद मिली होगी, क्योंकि इसी वर्ष पश्चिम पंजाब के शासक क्षत्रप यूदेमस (Eudemus) ने अपनी सेनाओं सहित, भारत छोड़ा। चंद्रगुप्त के यवनयुद्ध के बारे में विस्तारपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सफलता से उन्हें पंजाब और सिंध के प्रांत मिल गए।
चंद्रगुप्त मौर्य का संभवत: महत्वपूर्ण युद्ध नंदों के साथ उपरिलिखित संघर्ष के बाद हुआ। जस्टिन एवं प्लूटार्क के वृत्तों में स्पष्ट है कि सिकंदर के भारत अभियन के समय चंद्रगुप्त ने उसे नंदों के विरुद्ध युद्ध के लिये भड़काया था, किंतु किशोर चंद्रगुप्त के घृष्ट व्यवहार ने यवनविजेता को क्रुद्ध कर दिया। फलत:, प्राणरक्षा के निमित्त चंद्रगुप्त को वहाँ से भागना पड़ा। भारतीय साहित्यिक परंपराओं से लगता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के प्रति भी नंदराजा अत्यंत असहिष्णु रह चुके थे। महावंश टीका के एक उल्लेख से लगता है कि चंद्रगुप्त ने आरंभ में नंदसाम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही अपनी त्रुटि का पता चल गया और नए आक्रमण सीमांत प्रदेशों से आरंभ हुए। अंतत: उन्होंने पाटलिपुत्र घेर लिय और धननंद को मार डाला।
इसके बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में भी किया। मामुलनार नामक प्राचीन तमिल लेखक ने तिनेवेल्लि जिले की पोदियिल पहाड़ियों तक हुए मौर्य आक्रमणों का उल्लेख किया है। इसकी पुष्टि अन्य प्राचीन तमिल लेखकों एवं ग्रंथों से होती है। आक्रामक सेना में युद्धप्रिय कोशर लोग सम्मिलित थे। आक्रामक कोंकण से एलिलमलै पहाड़ियों से होते हुए कोंगु (कोयंबटूर) जिले में आए और यहाँ से पोदियिल पहाड़ियों तक पहुँचे। दुर्भाग्यवश उपर्युक्त उल्लेखों में इस मौर्यवाहिनी के नायक का नाम प्राप्त नहीं होता। किंतु, 'वंब मोरियर' से प्रथम मौर्य सम्राट् चंद्रगुप्त का ही अनुमान अधिक संगत लगता है।
मैसूर से उपलब्ध कुछ अभिलेखों से चंद्रगुप्त द्वारा शिकारपुर तालुक के अंतर्गत नागरखंड की रक्षा करने का उल्लेख मिलता है। उक्त अभिलेख 14वीं शताब्दी का है किंतु ग्रीक, तमिल लेखकों आदि के सक्ष्य के आधार पर इसकी ऐतिहासिकता एकदम अस्वीकृत नहीं की जा सकती।
चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र की विजय भी की थी। महाक्षत्रप रुद्रदामन् के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित है कि चंद्रगुप्त के राष्ट्रीय, वैश्य पुष्यगुप्त यहाँ के राज्यपाल थे।
चद्रंगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्वसेनापति तथा उनके समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट् सेल्यूकस के साथ हुआ। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के उल्लेखों से प्रमाणित होता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस को उसके स्वामी के सुविस्तृत साम्राज्य का पूर्वी भाग उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। सेल्यूकस, सिकंदर की भारतीय विजय पूरी करने के लिये आगे बढ़ा, किंतु भारत की राजनीतिक स्थिति अब तक परिवर्तित हो चुकी थी। लगभग सारा क्षेत्र एक शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में था। सेल्यूकस 305 ई.पू. के लगभग सिंधु के किनारे आ उपस्थित हुआ। ग्रीक लेखक इस युद्ध का ब्योरेवार वर्णन नहीं करते। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त की शक्ति के संमुख सेल्यूकस को झुकना पड़ा। फलत: सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को विवाह में एक यवनकुमारी तथा एरिया (हिरात), एराकोसिया (कंदहार), परोपनिसदाइ (काबुल) और गेद्रोसिय (बलूचिस्तान) के प्रांत देकर संधि क्रय की। इसके बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। उपरिलिखित प्रांतों का चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसके उततराधिकारियों के शासनांतर्गत होना, कंदहार से प्राप्त अशोक के द्विभाषी लेख से सिद्ध हो गया है। इस प्रकार स्थापित हुए मैत्री संबंध को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से सेल्यूकस न मेगस्थनीज नाम का एक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यह वृत्तांत इस बात का प्रमाण है कि चंद्रगुप्त का प्राय: संपूर्ण राजयकाल युद्धों द्वारा साम्राज्यविस्तार करने में बीता होगा।
श्रवणबेलगोला से मिले शिलालेखों के अनुसार, चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में जैन-मुनि हो गए। चन्द्र-गुप्त अंतिम मुकुट-धारी मुनि हुए, उनके बाद और कोई मुकुट-धारी (शासक) दिगंबर-मुनि नहीं हुए | अतः चन्द्र-गुप्त का जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोल चले गए। वहीं उन्होंने उपवास द्वारा शरीर त्याग किया। श्रवणबेलगोल में जिस पहाड़ी पर वे रहते थे, उसका नाम चंद्रगिरि है और वहीं उनका बनवाया हुआ 'चंद्रगुप्तबस्ति' नामक मंदिर भी है।सनातनी
साम्राज्य
चंद्रगुप्त का साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण-पश्चिम में सौराष्ट्र तक का विस्तृत भूप्रदेश सम्मिलित था। इनका साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिंद्कुश तक दक्षिणमें कर्नाटकतक पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक था साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी सम्राट् स्वयं था। शासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। प्रांतों के शासक सम्राट् के प्रति उत्तरदायी होते थे। राज्यपालों की सहायता के लिये एक मंत्रिपरिषद् हुआ करती थी। केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन के विभिन्न विभाग थे और सबके सब एक अध्यक्ष के निरीक्षण में कार्य करते थे। साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेश सड़कों एवं राजमार्गों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
पाटलिपुत्र (आधुनिक पटना) चंद्रगुप्त की राजधानी थी जिसके विषय में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज़ ने विस्तृत विवरण दिए हैं। नगर के प्रशासनिक वृत्तांतों से हमें उस युग के सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को समझने में अच्छी सहायता मिलती है।
मौर्य शासन प्रबंध की प्रशंसा आधुनिक राजनीतिज्ञों ने भी की है जिसका आधार 'कौटिलीय अर्थशास्त्र' एवं उसमें स्थापित की गई राज्य विषयक मान्यताएँ हैं। चंद्रगुप्त के समय में शासनव्यवस्था के सूत्र अत्यंत सुदृढ़ थे।
शासनव्यवस्था
चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की शासनव्यवस्था का ज्ञान प्रधान रूप से मेगस्थनीज़ के वर्णन के अवशिष्ट अंशों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से होता है (दे. मेगस्थनीज़)। अर्थशास्त्र में यद्यपि कुछ परिवर्तनों के तीसरी शताब्दी के अंत तक होने की संभावना प्रतीत होती है, यही मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री की कृति थी।
राजा शासन के विभिन्न अंगों का प्रधान था। शासन के कार्यों में वह अथक रूप से व्यस्त रहता था। अर्थशास्त्र में राजा की दैनिक चर्या का आदर्श कालविभाजन दिया गया है। मेगेस्थनीज के अनुसार राजा दिन में नहीं सोता वरन् दिनभर न्याय और शासन के अन्य कार्यों के लिये दरबार में ही रहता है, मालिश कराते समय भी इन कार्यों में व्यवधान नहीं होता, केशप्रसाधन के समय वह दूतों से मिलता है। स्मृतियों की परंपरा के विरुद्ध अर्थशास्त्र में राजाज्ञा को धर्म, व्यवहार और चरित्र से अधिक महत्व दिया गया है। मेगेस्थनीज और कौटिल्य दोनों से ही ज्ञात होता है कि राजा के प्राणों की रक्षा के लिये समुचित व्यवस्था थी। राजा के शरीर की रक्षा अस्त्रधारी स्त्रियाँ करती थीं। मेगेस्थनीज का कथन है कि राजा को निरंतर प्राणभ्य लगा रहता है जिससे हर रात वह अपना शयनकक्ष बदलता है। राजा केवल युद्धयात्रा, यज्ञानुष्ठान, न्याय और आखेट के लिये ही अपने प्रासाद से बाहर आता था। आखेट के समय राजा का मार्ग रस्सियों से घिरा होता था जिनकों लाँघने पर प्राणदंड मिलता था।
अर्थशास्त्र में राजा की सहायता के लिये मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था है। कौटिल्य के अनुसार राजा को बहुमत मानना चाहिए और आवश्यक प्रश्नों पर अनुपस्थित मंत्रियों का विचार जानने का उपाय करना चाहिए। मंत्रिपरिषद् की मंत्रणा को गुप्त रखते का विशेष ध्यान रखा जाता था। मेगेस्थनीज ने दो प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख किया है - मंत्री और सचिव। इनकी सख्या अधिक नहीं थी किंतु ये बड़े महत्वपूर्ण थे और राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। अर्थशास्त्र में शासन के अधिकारियों के रूप में 18 तीर्थों का उल्लेख है। शासन के विभिन्न कार्यों के लिये पृथक् विभाग थे, जैसे कोष, आकर, लक्षण, लवण, सुवर्ण, कोष्ठागार, पण्य, कुप्य, आयुधागार, पौतव, मान, शुल्क, सूत्र, सीता, सुरा, सून, मुद्रा, विवीत, द्यूत, वंधनागार, गौ, नौ, पत्तन, गणिका, सेना, संस्था, देवता आदि, जो अपने अपने अध्यक्षों के अधीन थे।
मेगस्थनीज के अनुसार राजा की सेवा में गुप्तचरों की एक बड़ी सेना होती थी। ये अन्य कर्मचारियों पर कड़ी दृष्टि रखते थे और राजा को प्रत्येक बात की सूचना देते थे। अर्थशास्त्र में भी चरों की नियुक्ति और उनके कार्यों को विशेष महत्व दिया गया है।
मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगरशासन का वर्णन किया है जो संभवत: किसी न किसी रूप में अन्य नगरों में भी प्रचलित रही होगी। (देखिए 'पाटलिपुत्र') अर्थशास्त्र में नगर का शसक नागरिक कहलाता है औरउसके अधीन स्थानिक और गोप होते थे।
शासन की इकाई ग्राम थे जिनका शासन ग्रामिक ग्रामवृद्धों की सहायता से करता था। ग्रामिक के ऊपर क्रमश: गोप और स्थानिक होते थे।
अर्थशास्त्र में दो प्रकार की न्यायसभाओं का उल्लेख है और उनकी कार्यविधि तथा अधिकारक्षेत्र का विस्तृत विवरण है। साधारण प्रकार धर्मस्थीय को दीवानी और कंटकशोधन को फौजदारी की अदालत कह सकते हैं। दंडविधान कठोर था। शिल्पियों का अंगभंग करने और जानबूझकर विक्रय पर राजकर न देने पर प्राणदंड का विधान था। विश्वासघात और व्यभिचार के लिये अंगच्छेद का दंड था।
मेगस्थनीज ने राजा को भूमि का स्वामी कहा है। भूमि के स्वामी कृषक थे। राज्य की जो आय अपनी निजी भूमि से होती थी उसे सीता और शेष से प्राप्त भूमिकर को भाग कहते थे। इसके अतिरिक्त सीमाओं पर चुंगी, तटकर, विक्रयकर, तोल और माप के साधनों पर कर, द्यूतकर, वेश्याओं, उद्योगों और शिल्पों पर कर, दंड तथा आकर और वन से भी राज्य को आय थी।
अर्थशास्त्र का आदर्श है कि प्रजा के सुख और भलाई में ही राजा का सुख और भलाई है। अर्थशास्त्र में राजा के द्वारा अनेक प्रकार के जनहित कार्यों का निर्देश है जैसे बेकारों के लिये काम की व्यवस्था करना, विधवाओं और अनाथों के पालन का प्रबंध करना, मजदूरी और मूल्य पर नियंत्रण रखना। मेगस्थनीज ऐसे अधिकारियों का उल्लेख करता है जो भूमि को नापते थे और, सभी को सिंचाई के लिये नहरों के पानी का उचित भाग मिले, इसलिये नहरों को प्रणालियों का निरीक्षण करते थे। सिंचाई की व्यवस्था के लिये चंद्रगुप्त ने विशेष प्रयत्न किया, इस बात का समर्थन रुद्रदामन् के जूनागढ़ के अभिलेख से होता है। इस लेख में चंद्रगुप्त के द्वारा सौराष्ट्र में एक पहाड़ी नदी के जल को रोककर सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख है।
मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के सैन्यसंगठन का भी विस्तार के साथ वर्णन किया है। चंद्रगुप्त की विशाल सेना में छ: लाख से भी अधिक सैनिक थे। सेना का प्रबंध युद्धपरिषद् करती थी जिसमें पाँच पाँच सदस्यों की छ: समितियाँ थीं। इनमें से पाँच समितियाँ क्रमश: नौ, पदाति, अश्व, रथ और गज सेना के लिये थीं। एक समिति सेना के यातायात और आवश्यक युद्धसामग्री के विभाग का प्रबंध देखती थी। मेगेस्थनीज के अनुसार समाज में कृषकों के बाद सबसे अधिक संख्या सैनिकों की ही थी। सैनिकों को वेतन के अतिरिक्त राज्य से अस्त्रशस्त्र और दूसरी सामग्री मिलती थीं। उनका जीवन संपन्न और सुखी था।
चंद्रगुप्त मौर्य की शासनव्यवस्था की विशेषता सुसंगठित नौकरशाही थी जो राज्य में विभिन्न प्रकार के आँकड़ों को शासन की सुविधा के लिये एकत्र करती थी। केंद्र का शासन के विभिन्न विभागों और राज्य के विभिन्न प्रदेशों पर गहरा नियंत्रण था। आर्थिक और सामाजिक जीवन की विभिन्न दिशाओं में राज्य के इतने गहन और कठोर नियंत्रण की प्राचीन भारतीय इतिहास के किसी अन्य काल में हमें कोई सूचना नहीं मिलती। ऐसी व्यवस्था की उत्पत्ति का हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। कुछ विद्वान् हेलेनिस्टिक राज्यों के माध्यम से शाखामनी ईरान का प्रभाव देखते हैं। इस व्यवस्था के निर्माण में कौटिल्य ओर चंद्रगुप्त की मौलिकता को भी उचित महत्व मिलना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था नितांत नवीन नहीं थी। संभवत: पूर्ववर्ती मगध के शासकों, विशेष रूप से नंदवंशीय नरेशों ने इस व्यवस्था की नींव किसी रूप में डाली थी।